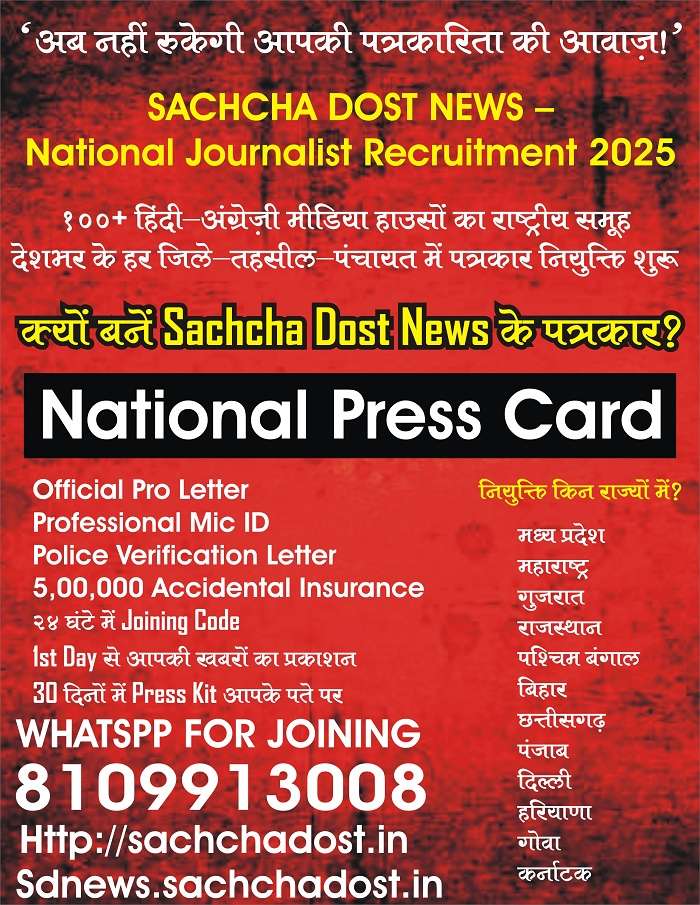नई दिल्ली: हिंदी भाषा में स्त्रीवाचक शब्दों के उपयोग और उनकी आवश्यकता पर बहस लंबे समय से चल रही है। आधुनिक युग में जहां महिलाएँ शिक्षा, राजनीति, खेल और हर पेशे में पुरुषों के साथ बराबरी कर रही हैं, वहां भाषा का पुराना ढांचा पितृसत्तात्मक नजर आता है। ‘बल्लेबाजिनी’, ‘निवेशिका’, ‘सैनिका’ जैसे नए शब्दों का प्रयोग कुछ अखबारों में शुरू हुआ, लेकिन सवाल उठता है: क्या इन शब्दों से समाज में वास्तविक समानता आएगी, या यह केवल भाषाई खेल बनकर रह जाएगा?
भाषा बनाम समाज
हिंदी का व्याकरण स्पष्ट है। “वह अच्छा डॉक्टर है” या “वह अच्छी डॉक्टर है” से ही स्पष्ट हो जाता है कि बात पुरुष की है या महिला की। इंदिरा गांधी या द्रौपदी मुर्मु के लिए कभी ‘प्रधानमंत्राणी’ या ‘राष्ट्रपतिनी’ नहीं लिखा गया, फिर भी उन्हें सम्मान मिला। पद, पद ही रहता है – अध्यक्ष, संपादक, विधायक – पुरुष या महिला के लिए समान रूप से प्रयुक्त होता है।
समस्या शब्दों में नहीं, सोच में है
असल लड़ाई भाषा के शब्दों से नहीं, बल्कि समाज की सोच से है। हमारी मुहावरों, लोकगीतों और दैनिक बोली में स्त्री-विरोध और जातीय भेदभाव झलकता है। मुहावरे और गालियाँ स्त्रियों का अपमान करती हैं, दलितों और पिछड़े वर्गों के लिए अपमानजनक शब्द हैं। वास्तविक बराबरी के लिए पितृसत्ता की जड़ पर हमला जरूरी है, न कि केवल शब्द बदलना।
बराबरी की दिशा में कदम
भाषा को सहज और सरल रखना चाहिए। लिंग निरपेक्ष शब्द स्वीकार्य हैं, लेकिन समाज में महिलाओं को सम्मान देने के लिए व्यापक प्रयास जरूरी हैं। महिला खिलाड़ी, निवेशक या नेता को अलग शब्द देने से अधिक प्रभावी तरीका है कि समाज उन्हें पुरुषों के बराबर अधिकार और सम्मान दे। अंग्रेज़ी शब्दों के अनावश्यक प्रयोग से बचें, व्याकरण और हिंदी की आत्मा को बनाए रखें।
निष्कर्ष
भाषा की लड़ाई समाज की लड़ाई के साथ चलती है। बराबरी की भाषा तभी असरदार होगी जब समाज में स्त्रियों को समान अधिकार, सम्मान और अवसर मिलें। शब्दों से खिलवाड़ नहीं, सोच में बदलाव की जरूरत है। पितृसत्ता की जड़ पर प्रहार कर ही महिलाओं को वास्तविक बराबरी दिलाई जा सकती है।